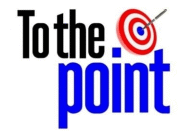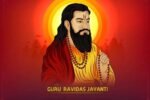भारत का किसान अपनी मेहनत की फसल का मूल्य खुद तय करने का हक रखता है, पर आज भी यह अधिकार उससे छीन लिया गया है। यह ब्लॉग MSP, कृषि सुधार, भारतीय कृषि नीति और APMC कानून की खामियों पर गहराई से चर्चा करता है। इसमें बताया गया है कि किसान की आय क्यों नहीं बढ़ पा रही और उसे सशक्त बनाने के लिए क्या कदम जरूरी हैं। किसान अधिकार, खेती का मूल्य और कृषि बाजार में पारदर्शिता ही आत्मनिर्भर भारत की असली नींव हैं। समय आ गया है किसान को उसका वास्तविक मूल्य और सम्मान लौटाने का।
किसान को अपनी पैदावार का मूल्य तय करने का हक क्यों नहीं? – भारत के कृषि तंत्र की वास्तविकता और समाधान

किसान का हक और उसकी हकमारी – असली सवाल क्या है?
भारत में “जय जवान जय किसान” का नारा आज भी गूंजता है, लेकिन हकीकत में किसान को अपनी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलता। हर व्यक्ति अपनी बनाई या बेची वस्तु का दाम खुद तय कर सकता है, फिर किसान को अपनी पैदावार का मूल्य तय करने का अधिकार क्यों नहीं? यही वह सवाल है जो भारत की कृषि व्यवस्था के केंद्र में है।
किसान अपनी मेहनत, पसीने और जोखिम से फसल तैयार करता है, परंतु उसकी कीमत तय करने का हक मंडियों, बिचौलियों और सरकारी नीतियों के पास है। यह हकमारी सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक अन्याय भी है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) के अनुसार, भारत में औसत किसान की मासिक आय लगभग ₹10,218 है, जिसमें से 60% हिस्सा खेती से नहीं, बल्कि अन्य कामों से आता है। इससे स्पष्ट है कि किसान अपनी मुख्य उपज से जीविका भी नहीं चला पा रहा है।
किसान अपनी वस्तुओं का मूल्य क्यों तय नहीं कर पाता? – पाँच मुख्य कारण
भारत का किसान अपनी पैदावार का मूल्य तय करने में असमर्थ है, इसके पीछे कई जटिल कारण हैं:
1. बाजार निर्भरता और बिचौलिया व्यवस्था:
किसान सीधे ग्राहक तक नहीं पहुँच पाता। मंडियों में बिचौलियों के कारण उसे फसल का न्यूनतम मूल्य भी नहीं मिलता। उदाहरण के लिए, गेहूँ जो बाजार में ₹28 प्रति किलो बिकता है, किसान को केवल ₹19–₹20 प्रति किलो तक ही मिलता है।
2. MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की सीमित पहुँच:
भारत सरकार लगभग 23 फसलों के लिए MSP तय करती है, लेकिन NITI Aayog की रिपोर्ट के अनुसार केवल 6% किसान ही MSP का वास्तविक लाभ उठा पाते हैं। बाकी किसान बाजार मूल्य पर फसल बेचने को मजबूर होते हैं।
3. भंडारण और लॉजिस्टिक की कमी:
किसान के पास अपनी उपज को सुरक्षित रखने की सुविधा नहीं है। ICAR रिपोर्ट 2024 के मुताबिक हर साल करीब ₹92,000 करोड़ की कृषि उपज भंडारण की कमी से खराब हो जाती है।
4. कृषि कानून और मंडी नियंत्रण:
पुराने APMC कानून के तहत किसान केवल निश्चित मंडियों में ही फसल बेच सकता है। इससे प्रतिस्पर्धा कम होती है और व्यापारी मनमाने दाम तय करते हैं।
5. तकनीकी जानकारी और वित्तीय साक्षरता की कमी:
अधिकांश किसान बाजार की मांग, लागत गणना या अंतरराष्ट्रीय मूल्य प्रणाली से अनजान रहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वे कम दाम पर अपनी फसल बेचने को मजबूर होते हैं।

सुधार की दिशा – किसानों के अधिकार और कृषि तंत्र में बदलाव की ज़रूरत
अगर भारत को “विकसित राष्ट्र” बनना है तो किसान को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना अनिवार्य है। इसके लिए निम्नलिखित सुधार जरूरी हैं:
MSP को कानूनी अधिकार बनाया जाए:
MSP सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि कानून बनना चाहिए, ताकि कोई व्यापारी किसान से कम मूल्य पर फसल न खरीदे।
डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म का विस्तार:
e-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) जैसी योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर मजबूत किया जाए, ताकि किसान सीधे खरीदार से संपर्क कर सके और ऑनलाइन मूल्य तय कर सके।
भंडारण और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर:
हर पंचायत स्तर पर मिनी कोल्ड स्टोरेज और गोदाम बनाए जाएं ताकि किसान अपनी फसल उचित समय पर उचित दाम में बेच सके।
कृषि सहकारी मॉडल:
अमूल जैसी सहकारी समितियों की तरह फसल आधारित सहकारी समितियाँ बनें जो किसानों को बाजार में सामूहिक रूप से बेहतर मोलभाव का अधिकार दें।
कृषि बीमा और लागत नियंत्रण:
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पारदर्शी बनाया जाए और बीमा क्लेम जल्दी निपटाए जाएं ताकि किसान का आर्थिक नुकसान कम हो।
किसान की आय दोगुनी कैसे होगी? – आत्मनिर्भर कृषि की राह
भारत सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन NABARD की 2023 रिपोर्ट बताती है कि अभी भी यह लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं हुआ। अब जरूरत है कि नीति और धरातल पर कार्यान्वयन एक साथ हो।
मूल्य आधारित खेती (Value-based Farming):
सिर्फ गेहूं-धान नहीं, बल्कि मसाले, फल, सब्ज़ियाँ, औषधीय पौधों और जैविक खेती पर ध्यान दिया जाए, जिससे किसान को बाजार में प्रीमियम मूल्य मिले।
प्रोसेसिंग यूनिट्स और कृषि उद्योग:
गाँवों में छोटे पैमाने के फूड प्रोसेसिंग सेंटर खोलकर किसानों को फसल के बाद मूल्यवर्धन का लाभ मिले। जैसे, टमाटर से सॉस बनाना, आलू से चिप्स बनाना आदि।
निर्यात उन्मुख नीतियाँ:
भारत का कृषि निर्यात FY 2024 में ₹4.17 लाख करोड़ रहा, लेकिन यह कुल कृषि उत्पादन का केवल 13% है। निर्यात को 25% तक बढ़ाया जाए तो किसानों की आय स्वतः दोगुनी हो सकती है।

शिक्षा और तकनीकी ज्ञान:
किसानों को डिजिटल प्रशिक्षण, मोबाइल ऐप्स और मार्केट रिपोर्टिंग टूल्स की मदद से यह सिखाया जाए कि बाजार कैसे चलता है और सही समय पर फसल कैसे बेची जाए।
🌾 निष्कर्ष: “किसान को दाम तय करने का हक दो, तो देश को विकास मिलेगा”
भारत का किसान केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जब तक किसान अपनी मेहनत की कीमत खुद तय नहीं करेगा, तब तक उसकी गरीबी और संघर्ष खत्म नहीं होंगे। कृषि सुधारों का असली मतलब तभी सफल होगा जब किसान के हाथ में अपनी उपज का मूल्य तय करने की शक्ति होगी।
अगर किसान समृद्ध होगा, तो देश भी आत्मनिर्भर और समृद्ध बनेगा।
Writer – Sita Sahay